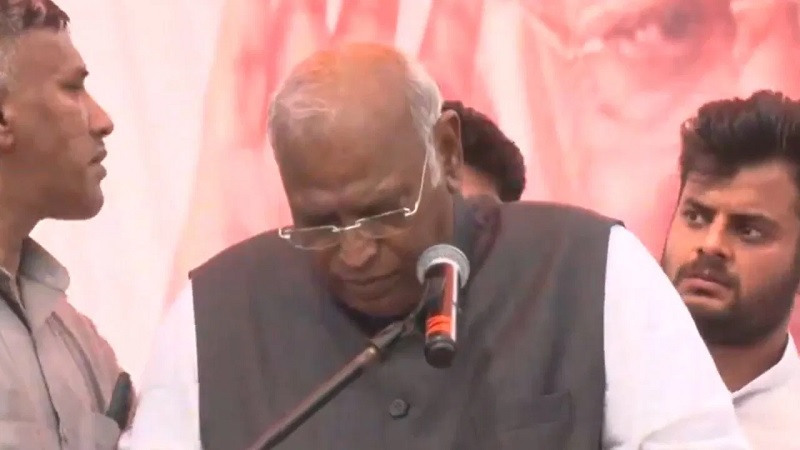(शम्सुर्रहमान फारूकी के जन्मदिन पर यादगार)
द लीडर : बनाएंगे नई दुनिया हम अपनी, तिरी दुनिया में अब रहना नहीं है…उर्दू अदब के नामवर साहित्यकार शम्सुर्रहमान फारूकी का ये शेर शुक्रवार को हकीकत बन गया. ये दुनिया उन्हें रास नहीं आई और अपने शेर को जीते हुए वे अलविदा कह गए.
30 सितंबर 1935 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में जन्मे फ़ारूक़ी अपने 85 साल के सफर में वे उर्दू अदब के क्षितिज सूरज की तरह चमकते रहे.
साल 1991 से लेकर 2004 तक वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसलवानिया, फिलाडेल्फिया (यूएसए) में मानद प्रोफ़ेसर रहे। बुनियादी तौर पर अंग्रेजी अदब के स्टूडेंट रहे फ़ारूक़ी 19वीं सदी के उर्दू अदब को नई ऊंचाईयों पर ले गए
(Shamsulrahman Faruqi Passed Away)

फारूकी को कहानी सुनाने की कला यानी दास्तानगोई को जिंदा करने का भी श्रेय दिया जाता है. उर्दू जगत के साहित्यकार डा. शम्स बदायूंनी कहते हैं कि उनका जाना साहित्य जगत का बड़ा नुकसाान है. उनके साहित्यिक सफर को याद करते हुए वह कहते हैं कि, ‘फारूकी हमारे दौर के उन साहित्यकारों में से थे, जो पूरबी और पश्चिमी दोनों साहित्य पर गहरी नजर रखते थे. वो सिर्फ तनकीद निगार (समालोचक) ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन तखलीककार (रचयिता) भी थे. उन्होंने उर्दू अदब को नये आयाम से रूबरू कराया. आले अहमद सुरूर के बाद वो पहले नाकिद (समालोचक) थे, जिनको संजीदगी से पढ़ा भी गया और सबसे ज्यादा हवालों में कोट किया गया. (Shamsulrahman Faruqi Passed Away)
इसे भी पढ़ें : किसान आंदोलन में विद्युत संशोधन विधेयक भी निशाने पर क्यों है
उन्हें कदीम (पुराने) और जदीद (नये) दोनों हल्कों में एक जैसा दर्जा हासिल था. उनका नॉबेल ‘कई चांद थे सरे आसमां’ पुराने और नये दोनों मानकों पर खरा उतरता है. और इस नॉबेल ने नये दौर में वो मुकाम हासिल किया है, जिस पर दूसरे उपन्यासकार भी रश्क कर सकते हैं. सबसे अहम बात यह है कि मीर की शायरी में अवाम की जुबान का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है. फारूकी से पहले मीर को जो समझने की कोशिश की गई, वो सिर्फ फन के एतबार तक सीमित दिखती है. लेकिन शम्सुर्रहमान फारूकी ने मीर की शायरी को अवाम तक पहुंचाने में सबसे अहम किरदार निभाया है. उनकी एक किताब-शेर व शोरअंगेज जो चार जिल्दो में है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है.’
उन्होंने अपनी पत्रिका शब-खून के जरिये साहित्य को बुलंदी पर पहुंचा दिया. साहित्य के इस मुसाफिर की जिंदगी का सफर प्रतापगढ़ में 15 जनवरी 1936 को शुरू हुआ था, जो शुक्रवार को इलाहाबाद में थम गया. अपने इस सफर में उन्हें डाक विभाग से लेकर पेंस्लिवेनिया यूनिवर्सिटी तक अपनी सेवाएं भी दीं.