कोरोना की दूसरी लहर से दहशत, अकेलेपन, तनाव, अवसाद का माहौल है। हर कोई कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके पास महफिल के नाम पर सोशल मीडिया है या कुछ लोगों से फोन पर बात करके मन का बोझ कम करने की कोशिश की जा रही है। नुस्खे और तसल्ली की झड़ी लगी है, हालांकि भरोसा फिर भी नहीं है। बहुत से लोग अंदर से टूट गए हैं। व्यवा कथा हर किसी के पास कम या ज्यादा है। इन हालातों में पढ़िए अभिषेक श्रीवास्तव के ये अनुभव और विचार, जो शायद सभी के मन का हाल है।
(एक)
दिल्ली लौटते ही दो दिन में दो दर्जन करीबी मित्रों की बीमारी और भर्ती की खबर मिली। घर में भी मां बीमार हैं दस दिन से। अपने कमरे में आइसोलेट हैं। विस्तारित परिवार में भी अधिकतर बीमार पड़े हैं। पत्नी जी बीमार हो के ठीक हो चुकी हैं लेकिन छुट्टी पर हैं। उनका पूरा दफ्तर ही संक्रमित है। एक कर्मचारी कल निपट गया। एक मित्र के पिता निकल लिए। कुछ पिता और हैं कतार में। एक मित्र की बहन और फूफा भर्ती हैं। चौतरफा घेराव लगता है अबकी। हिट एंड ट्रायल का गेम है। कोई विज्ञान नहीं। सब तुक्का है। बच गए तो जय श्री राम, निकल लिए तो हे राम।
इतने सघन संकट के बीच अकेले में यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल लग रहा है कि अबकी पिछली बार जैसा न डर है, न चिंता, न दुख, न उत्तेजना और न ही कोई चिंतन। यह नियतिवाद है या न्यू नॉर्मल या जोम्बीकरण, पता नहीं। ऐसा लगता है कि पहले सारा काम निपटा लें, जाने कब नंबर आ जाए। फिर लगता है कि पेंडिंग कामों से फारिग हो लेने के बाद अवसर मिलेगा तो थोड़ा दुखी भी हो लेंगे। चिंता कर लेंगे। इस बात पर आज हंसी भी आ रही थी। फिर याद आया पिछले साल का समय, जब मैंने लिखा था कि मानवीय त्रासदी के बाद मनुष्य और निर्मम, कठोर, अमानवीय हो जाता है।
चाहे जो हो, लेकिन एक ही नदी में दो बार हाथ नहीं धोया जा सकता। अनुभूत को नया अनुभव नहीं बनाया जा सकता। सोचता हूं, काश, इस नए स्ट्रेन और दूसरी लहर का नाम कुछ और होता। थोड़ा भयावह टाइप। जैसे, मरो-ना! थोड़ा किक आती। फिर भी, एक कामना जरूर है कि इस बार अच्छे लोग बच रहें, पापी निपट जाएं। कुछ खास लोग 2 मई का सूरज न देखने पाएं। क्या ही अच्छा हो। निस्सहायता में सैडिस्ट प्लेज़र बहुत काम की चीज है। ये पिछली बार नहीं था। अबकी तगड़े से है। आदमी ऐसे ही जोम्बी बनता होगा।
यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया ज्ञान नहीं, इस जमीनी सच से हों वाकिफ
(दो)
पिछले 72 घंटे में ऐसा हुआ है, जैसे पहले ही एक तीर लगने से अवाक, घायल और क्षुब्ध पीठ पर दूसरा तीर आ लगा हो। इसमें दुख नहीं है, सघन और केंद्रीभूत पीड़ा है जो भीतर से लहर मार रही है। सांस की कमी की खबरें सुन-सुन के एक दोस्त का दम घुटने लगा, उसे पैनिक अटैक हो गया। जीटीबी अस्पताल में 500 लोग ऑक्सीजन के सहारे हैं और चार घंटे की सप्लाई बची है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ट्विटर पर यह सूचना देते हुए केंद्र से अपील कर रहे हैं, इस बात को भूलकर कि कल रात खुद उनकी बेरुखी से एक डॉक्टर की मौत हो गई थी।
दवा, बिस्तर और ऑक्सीजन के लिए लगातार यहां-वहां से आ रहा हर एक फोनकॉल “मैं” की लघुता से आपका साक्षात्कार करवाता है। आप आश्वासन देने से लेकर धरा-व्योम को एक करने वाला भगीरथ प्रयास करते हैं। संपर्कों से बदहवास प्रार्थनाएं करते हैं। सब जगह से उम्मीद सिमट कर आप तक आते-आते दहलीज पर दम तोड़ देती है। इसके ठीक बाद एक आदमी मर जाता है। कल एक मित्र के परिजन, एक की मां, एक के पिता, सब चले गए। “मैं” कुछ नहीं कर सका क्योंकि “मैं” था ही नहीं कभी। केवल वहम था, उसके होने का।
अब, जबकि प्याज छीलते-छीलते अंततः कुछ बरामद नहीं हुआ है, तो अन्नमय से लेकर विज्ञानमय तक फैली पांचों अंतरगुंफित गुफाएं सन्नाटे में भांय-भांय कर रही हैं। समझना मुश्किल है ये “मैं” होता ही नहीं या “मैं” ही सब कुछ होता है। नहीं होता तो देखने वाला भी नहीं होता, न अनुभूत करने वाला। इसलिए “मैं” है तो, लेकिन द्रष्टा भर। और देखना, दूसरे तीर को पीठ पर लेने जैसा है। किसी ऐसे ही क्षण में मिल्टन की आंख चली गयी होगी। ‘अजीब दास्तान’ में बेजुबान मानव कौल का आखिरी सांकेतिक डायलॉग सच हुआ होगा- “तुमने तो अपनी आंखों से भी झूठ बोल दिया!”
यह भी पढ़ें: दूसरी लहर कब खत्म होगी, क्या और लहरें आना बाकी हैं?
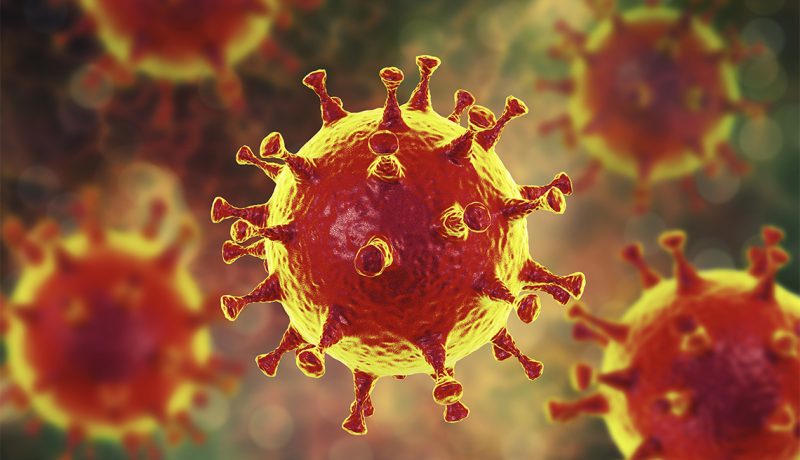
(तीन)
संकट केवल बिस्तर, सांस और दवा का नहीं है। आपके पास इन सब की सही सही सूचना हो भी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मसलन, दिल्ली में ऑन रिकॉर्ड 18 बिस्तर खाली हैं। 11 मालवीय नगर, 3 नजफगढ़, 3 दिल्ली कैंट, 1 ट्रॉमा सेन्टर में। अब आप हाथ पैर मारना शुरू करते हैं। आधा घंटा चारों के नंबर मिलाते हैं। दो निरंतर व्यस्त, एक पहुंच से बाहर, चौथा स्विच ऑफ। फिर वैकल्पिक नंबर खोजते हैं। मिलाते हैं। वही हाल।
फिर दो लोग मिल के बारी-बारी से व्यस्त नम्बरों को मिलाते हैं आधे घंटे तक। एक नंबर लग गया। धन्य हुए। हेलो? सर, बिस्तर तो है लेकिन महिला और बच्चे के लिए, लेकिन महिला प्रेग्नेंट होनी चाहिए। भाई साहब, बुज़ुर्ग महिला है, ले लीजिए भर्ती! नहीं सर, प्रेग्नेंट होना ज़रूरी है। अद्भुत बात! मतलब, मुंह से गाली भी न निकल सके ऐसा तर्क!
सवा घंटे पर दूसरा फोन उठता है। जीवन धन्य। बेड? नहीं सर। लेकिन उपलब्ध दिखा रहा है तीन। क्या बताएं सर, तीन घंटे से ऑनलाइन जीरो अपडेट करने को कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो ही नहीं पा रहा। अच्छा? मतलब जो मैंने देखा वो रियल टाइम उपलब्धता नहीं है? नहीं सर। मने, मैं तीन घंटे से मतलब…? मुंह से अपशब्द नहीं निकले, अटक गए। सर… जी? डीआरडीओ में देख लीजिए। नंबर दीजिए। वो तो नहीं है। कहां मिलेगा? पता नहीं सर।
वो नंबर ट्विटर पर हर जगह अलग अलग नामों से मौजूद है। ट्वीट करने वाले अपने को सूचना को दुनिया का मोगाम्बो समझे बैठे हैं। ज़रा नंबर लगा के देखिए। लग जाए तो कसम ऑक्सीजन की…!
यह भी पढ़ें: सुई में ऊंट कैसे डाला जाए? पढ़कर आप भूल जाएंगे कोरोना से मिले गम
(चार)
आज शाम अचानक एक पुराना गाना याद आया- “नज़रों के तीर मारे कस कस कस / एक नहीं दो नहीं आठ नौ दस”। संदर्भ अब तक नहीं सूझ रहा, कि कैसे और क्योंकर ये गाना कौंधा दिमाग में। फिर लगा कि आठ नौ दस तीर किसी को लग जाए तो वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें का दर्द तो भूल जाता होगा! दसवां लगते ही आठवें और नौवें की भी याद नहीं रहती होगी! और इतने तीर खाने के बाद ग्यारहवें, बारहवें की आशंका में दसवें से भी दिमाग हट जाता होगा! नहीं?
किस किस को रोया जाय? रेणु अगाल मेरे जीवन में मेरी पहली कमीशनिंग एडिटर थीं। उनकी कमीशन की हुई किताब आज तक नहीं छपी। अक्सर पूछती थीं, क्या हुआ। अम्बरीष राय से बीस साल पुराना नाता था। जब भी फोन करते, मेरा कुछ न कुछ लिखा पढ़ने के बाद ही करते और फिर उस पर बात करते। उन्हें अंत तक अफसोस रहा कि उन्होंने बरसों पहले मुझे एक नौकरी नहीं दी। उत्तर आधुनिकता पर पहला टेक्स्ट हिंदी में रमेश उपाध्याय का पढ़ा था मैंने बरसों पहले, फिर बात होने लगी थी। अजित साहनी ने 2016 दिसंबर में समकालीन तीसरी दुनिया को जिंदा रखने के लिए भरी सभा में छाती ठोक के एक करोड़ जुटाने का ढांढस हमें बंधाया था। दिलीप के रिसेप्शन में आखिरी बार मिला था। बातें ही बातें हैं। लोग ही लोग। यही हम सब की कमाई रही है। किस किस को खोया जाय?
एक समय में हिंदी में एक मुहावरा चलता था “नपुंसक आक्रोश”। फिर लोग थोड़े उपभोक्ता हुए तो कवियों ने इसे “नपुंसक गुस्सा” लिखना शुरू कर दिया। फिर ये भी जाता रहा। गुस्से को जज़्ब करने के बाद उपजने वाला दुख होने लगा कुछ बरसों तक। फिर आया राम राज्य। एकदम रामायण सीरियल की तर्ज़ पर एक तीर उधर सिस्टम से छूटा, इधर दस तीर में बंट के आ लगा एक के बाद एक कस कस कस। आठ नौ दस। इससे उपजे भाव को व्यक्त करने में कविता असमर्थ हो गई क्योंकि तब तक कविता चॉकलेट बन चुकी थी जिसे दूसरों का स्टेटस देखते हुए सब रियल टाइम में चुभला रहे थे।
याद आया, अपने जीते जी कविता को चॉकलेट बनता देखने वाले और अपनी एक कविता में पहली बार ऐसा कहने वाले बांग्ला कवि शंख घोष भी नहीं रहे। कविता जैसी फ़िल्म रचने वाली सुमित्रा भावे चुपचाप चली गईं। ऐसे तमाम लोग थे जिनकी ज़िंदगी जितना शांत थी, मौत उससे कहीं ज़्यादा शांत रही। अपने आसपास बहुत से लोग जा रहे हैं, लगातार, और मुझे मंगलेश जी याद आ रहे हैं जो इस आक्रोशहीन और दुखहीन भाव पर हिंदी में सबसे सुंदर लिख सकते थे। आज दुख के बारे में सच लिखने वाला, उसे सही मुहावरा देने वाला, कोई नहीं है। “सैयां मैं तो हार गई बस बस बस…”- नायिका घबरा कर सिस्टम से इसके सिवा और कह भी क्या सकती हैै? किस-किस को रोया जाय? किस-किस को खोया जाय?
यह भी पढ़ें: अथ कोरोना कथा: कोई सीधी रेखा नहीं है जीवन – जितेंद्र श्रीवास्तव की कविताएं
(पांच)
दुखी होना affordability का मसला है। Affordability के लिए अच्छी हिन्दी खोजना मुश्किल है, शायद यहां कोई बता पाए। ‘वहनीयता’ में वो बात नहीं है। दुख का ‘वहन’ कहने से लगता है गोया दुखी आदमी कोई वाहन हो और दुख उसके कंधे पर सवार हो। फिर भी, इसी को चलने देते हैं। दुख का जो वाहन न बन सके, उसे कंधे से तत्काल झाड़ फेंके, वो अपेक्षया जड़ हो जाता है। जड़ व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। इसलिए वो जी जाता है। दुखी हुए तो समझो गए। सटला त गईला बेटा टाइप!
जैसे गरीब। मेरा एक दोस्त कह रहा था परसों कि कोरोना से उसे गरीबी ने बचा लिया। उसे जब लगा कि अस्पताल चला जाए, तो उसने सोचा कि इतना पैसा कहां से आएगा। फिर ईएमआइ भरनी है, कर्जा भी बहुत है। फिर उसने फैसला किया कि गरीबी में आटा गीला हो जाएगा इसलिए भर्ती नहीं होना, घर पर ही रहना है। वो ठीक हो गया। उसने सुख का वहन नहीं किया। सुख का वहन करता तो निपटने का खतरा था। सुख उसके लिए affordable नहीं था। गरीबी ने जान बचा ली।
गरीबी affordable है। जड़ता affordable है। गरीब का अपनी चादर फाड़ के सुखी होना जानलेवा है। जैसे दुखी होना। सुख-दुख दोनों जान ले सकते हैं। गरीबी आपको जड़ बना देती है। जड़ता ही सच्ची गरीबी है। दुख वहां नदारद है। इसीलिए गरीब कविता नहीं करता। कविता उनके लिए है जो दुखी होना afford कर सकें। जो दुख का वाहन बन सकें। जो कवि सुख भी afford कर पाता है, उसकी कविता चॉकलेट बन जाती है। जो सुख और दुख दोनों को afford नहीं कर पाता और इस मामले में अपनी औकात जानता है, वो पार लग जाता है। बड़े आराम से!
यह भी पढ़ें: इतने खौफजदा क्यों हैं हम, सच्चाई के इस पहलू को भी जानना चाहिए
(छह)
किसी भी दौर में सबसे ज़्यादा कोफ्त मुझे मध्यवर्ग से होती है। अद्भुत बुनावट है इस तबके की। अजीब मुगालते हैं। बीते पांच दिन में जो अनुभव रहे, उससे एक बात तो समझ आयी है कि बी और सी ग्रेड के शहरों में इस वर्ग से जितने लोगों की मौत हो रही है और अब तक हुई है, ज़्यादातर मामले वर्गीय प्रवृत्ति से ताल्लुक रखते हैं।
पहली प्रवृत्ति- सीधे चलने के बजाय तिरकट्टे चलना। इसका आशय यह है कि ज़रूरत पड़ने पर सरकारी अस्पताल, प्रशासन, ज़िम्मेदार अधिकारियों से मुंह चुराना और पहले ही प्रयास में डायरेक्ट संपर्क खोजना है। दूसरी बुरी आदत है सीधे प्राइवेट संस्थानों का रुख करना। तीसरी प्रवृत्ति है ज़रूरत से ज़्यादा घबराना, दूसरे को घबरवाना, ‘मर जाएंगे’ टाइप गुहार लगाना और उस बहाने माल मटेरियल एडवांस में अपने पास जमा कर लेना। किसी संपर्क से कहीं कुछ जुगाड़ लग गया तो जांगर हिलाए बगैर घर पर सेवा पहुंच जाए, इस चक्कर में रहना। काम होने पर पलट के एक बार अपडेट तक नहीं करना।
इन सबका नतीजा- ऐन उस मौके पर विवेक और संयम का घास चरने चले जाना जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। उधर ही नहीं, इधर भी। जब दिन भर में एक साथ कई फाइलें खोल के आप बैठे हुए हों और दिन के अंत में कोई क्लोज़र रिपोर्ट तक दाखिल न करे, तो रात में बेचैनी होती है कि क्या हुआ होगा। कन्फर्म करने के लिए फोन करें, तो फोन न उठे। अजीब स्थिति है। एक तो कुछ न कर पाने का गिल्ट, दूसरा कुछ हो जाने की संभावना से जुड़ा अनिश्चयबोध।
आज एक मित्र कहानी सुना रहे थे एक संत और प्लेग की। संत मक्का से लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें प्लेग मिला। उन्होंने पूछा कहां जा रहे हो। मक्का- प्लेग ने कहा। संत ने पूछा कितने को मारने का टार्गेट है। उसने कहा- पांच हज़ार। सन्त बोले, ठीक है जाओ, अपना काम करो। अगले साल संत मक्का के लिए निकले तो रास्ते में प्लेग फिर मिला, लौट रहा था। संत ने पूछा- कितने मारे? प्लेग बोला पांच हज़ार। संत ने कहा- झूठ बोलते हो। हमने तो 50,000 की मौत सुनी थी? प्लेग गिड़गिड़ाते हुए बोले- क्यों बदनाम करते हो मौलाना? मैंने पांच हज़ार बोला था तुमसे, मैंने उतने ही मारे हैं। बाकी के 45000 तो दहशत से मर गए।
इसे अपने डॉक्टर साहब कुछ यूं कहते हैं कि नाली से अठन्नी निकालने के लिए 100 रुपया खर्च कर देना और अठन्नी भी न निकले। कोरोना की इस लहर में शहरी मध्यवर्ग को हो रहे नुकसान का यही सार है। अठन्नी के संकट ने 100 रुपये की दहशत पैदा कर दी है। ये वही दहशत है जिसे हम बम्बई में पुल टूटने या किसी बाबा के आश्रम में हुई भगदड़ में देख चुके हैं पहले। इसमें आदमी अचानक भीड़ बन जाता है। सब एक तरह से सोचते हैं, एक ही काम करते हैं। यही एकरंगी मध्यवर्गीय भीड़ अब तक घेर कर अकेले शख्स को मारती आई है। आज अपने जान की दुश्मन बन के खुदकुशी करने पर आमादा है। दहशत और उससे पैदा हुई विवेकहीनता में हत्या और आत्महत्या दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं।
सात साल बाद शहरी मध्यवर्ग ने पहली बार पहलू बदला है। आज वो अपनी जान का दुश्मन बना बदहवास घूम रहा है। समाज और देश के नियंता उसका चरित्र बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए हांक भी लेते हैं जिधर चाहे उधर। इसीलिए मैं अपने कुछ दोस्तों की तरह कतई आशावादी नहीं हूं कि इतने बड़े पैमाने की मानवीय त्रासदी किसी तरह की राजनीतिक-सामाजिक जागरूकता या सहकार और नागरिक कर्तव्य का अहसास पैदा कर पायेगी।
(अभिषेक श्रीवास्तव जनपक्षधर पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में जानी मानी शख्सियत हैं, उपरोक्त श्रृंखला उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रकाशित की हैं)
(आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)





